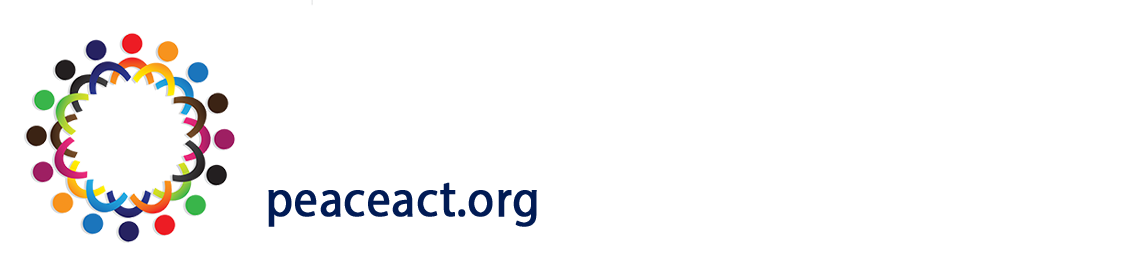आज के समय में जलवायु परिवर्तन और बेरोजगारी के मुद्दे हमारे सामने मुंह बाए खड़े हैं, इनसे निपटने के लिए सुप्रीमकोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं, लेकिन किन्हीं अनजानी गफलतों, हितों या भूल जाने की राष्ट्रीय बीमारी के चलते उन्हें अमल में नहीं लाया जा रहा। क्या हैं ये फैसले? और दुनिया-जहान को हलाकान करने वाले इन दोनों मुद्दों को इनसे कैसे हल किया जा सकता है? ‘गणतंत्र दिवस’ पर अपने विशेष लेख में बता रहे हैं, राहुल बनर्जी;
मनुष्यों के सामने आज की सबसे बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन। कहा जा रहा है कि इसके चलते निकट भविष्य में मानव समेत विश्व की सभी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। मुख्य रूप से औद्योगिक विकास के लिए जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण हो रहे कार्बन डाइआक्साइड व अन्य गैसों के उत्सर्जन से तापमान में वृद्धि ने यह संकट पैदा किया है। वर्ष 2024 तक तापमान वृद्धि औद्योगिक क्रांति के पूर्व के मुकाबले 1.5 डिग्री सेंटिग्रेड हो गई है और यह हर दशक 0.2 डिग्री सेंटिग्रेड की दर से बढ़ रही है। आशंका है कि यह वृद्धि 2050 तक 2 डिग्री सेंटिग्रेड हो गई तो जलवायु परिवर्तन के भीषण परिणाम होंगे जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन ही खत्म होना शुरू हो जाएगा।
फिलहाल हर वर्ष दुनिया में 42 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें पेड़-पौधों एवं समुद्री शैवाल के द्वारा से केवल 2 अरब टन का वापस अवशोषण हो रहा है। इस समस्या से निजात पाने का केवल एक ही उपाय है – जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद कर दिया जाए एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा-स्त्रोत, जैसे सौर-वायु ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। इस दिशा में प्रगति के लिए भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई है जिसके दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य हो रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ‘संयुक्त राष्ट्र संघ’ ने जलवायु परिवर्तन पर एक संवाद जारी रखा है जिसके तहत हर वर्ष बैठकें होती हैं जिनमें कार्बन उत्सर्जन कम करने के लक्ष्य तय किए जाते हैं एवं सभी देशों को उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कदम उठाने होते हैं। इसी के तहत भारत सरकार ने भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने की योजना बनायी है। कानूनी तौर पर ‘भारतीय विद्युत अधिनियम’ में प्रावधान किये गए हैं कि विद्युत उत्पादन अधिक-से-अधिक पुनर्नवीकरणीय स्त्रोतों से हो। यातायात नियमों में भी प्रावधान किए गए हैं कि अधिक-से-अधिक वाहन पुनर्नवीकरणीय स्त्रोतों से उत्पादित विद्युत पर चलें। इसके अलावा सभी उद्योगों के लिए दिशा-निर्देश तय किए गए हैं कि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने के कारगर कदम उठाएं। इसके लिए वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुछ प्रकरणों में महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण, विशेषकर जलवायु परिवर्तन की रोकथाम को भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार का दर्जा प्राप्त हो गया है। इनकी चर्चा बहुत उपयोगी साबित होगी। दीवानी याचिका क्र 838/2019 में कुछ पर्यावरणवादियों ने सर्वोच्च न्यायालय में यह आवेदन किया था कि राजस्थान और गुजरात में स्थापित विशाल सौर-ऊर्जा संयंत्र के तारों में उलझकर ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ नामक पक्षी मर रहे हैं और इसलिए इस विलुप्तप्राय प्रजाति को बचाने के लिए इनके निवास क्षेत्र में तारों से विद्युत पारेषण बंद कर भूगर्भ केबल के माध्यम से किया जाए।
इस पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2021 में निर्णय दिया था कि संविधान की धारा 21 में प्रदत्त जीने का अधिकार केवल मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि सभी प्रजातियों के लिए है। यह इसलिए क्योंकि मनुष्य अकेला जी नहीं सकता, बल्कि प्रकृति के तमाम जीवों के साथ उसे जीना होगा। यानि मानव केंद्रित न्याय के बदले प्रकृति केंद्रित न्याय को अपनाना होगा। इसलिए उस समय के अंतरिम निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश दिया गया था कि तारों से विद्युत पारेषण बंद कर भूगर्भ से पारेषण किया जाए।
इस निर्णय के विरुद्ध सौर-ऊर्जा कंपनियों एवं केंद्र सरकार ने अपील की कि भूगर्भ केबल बहुत मंहगा है एवं उससे पारेषण करने से सौर विद्युत की कीमत इतनी अधिक हो जाएगी कि उपभोक्ता उसे खरीद ही नहीं पाएंगे। इस प्रकार कार्बन उत्सर्जन को कम कर जलवायु परिवर्तन रोकने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा जिसके फलस्वरूप अंततः पृथ्वी की सभी जीवित प्रजातियों की विलुप्ति हो जाएगी। सन 2024 में इस तर्क को मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न वर्तमान संकट गंभीर है, इसलिए सभी प्राणियों के जीने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सौर-ऊर्जा का उत्पादन एवं पारेषण महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क के आधार पर कुछ सावधानियों के साथ तारों से सौर-ऊर्जा के पारेषण की अनुमति दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से जलवायु परिवर्तन के शमन को संविधान की धारा 21 के तहत ‘जीने के अधिकार’ का दर्जा प्राप्त हो चुका है।
हालांकि यह भी सोचने लायक है कि सौर-ऊर्जा का उत्पादन केवल विशाल संयंत्रों से ही क्यों किया जा रहा है, जबकि इसमें किसी भी अन्य केन्द्रीकृत उद्योग जैसी विस्थापन सरीखी बहुत सारी अन्य समाजार्थिक समस्याएं भी हैं। सौर एवं वायु ऊर्जा, कृषि या वन के जैव-अवशेषों से छोटे-छोटे समूहों में भी सामुदायिक स्तर पर ऊर्जा उत्पादन किया जा सकता है। इसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित विद्युत के उपयोग में तारों से पारेषण की आवश्यकता ही नहीं होगी, परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा क्योंकि इसमें उद्योगपतियों को मुनाफा नहीं होगा। नतीजे में सरकार पर दबाव डालकर उद्योगपतियों द्वारा अनुदान लेकर केन्द्रीकृत संयंत्रों में सौर-ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि सामुदायिक ऊर्जा उत्पादन का एक और फायदा यह भी है कि इससे व्यापक पैमाने पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पहले 1985 में ही निर्णय दिया था कि ‘रोजगार का अधिकार’ भी संविधान की धारा 21 के तहत ‘जीने के अधिकार’ का अंग है। इसी क्रम में ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005’ (मनरेगा) पारित किया गया जिसमें न केवल प्रत्येक इच्छुक वयस्क व्यक्ति को वर्ष में सौ दिन का रोजगार देने, बल्कि ऐसे कामों के लिए देने का प्रावधान है जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले, जैसे – भूमि, जल व वन-संरक्षण आदि। ‘मनरेगा’ को शहरों में भी लागू कर इससे व्यापक पैमाने पर सामुदायिक पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का काम भी किया जा सकता है। इससे जलवायु परिवर्तन के शमन एवं रोजगार सृजन के दोनों महत्वपूर्ण लक्ष्य बखूबी हासिल हो सकते हैं।
विडंबना यह है कि वर्तमान में ‘मनरेगा’ पर सरकारी निवेश बेहद कम है एवं औसतन वर्ष में केवल 9 दिन का रोजगार सृजन हो रहा है, वह भी भवन एवं सड़क निर्माण जैसे गैर-पर्यावरणीय क्षेत्रों में। अतः देश और दुनिया की भलाई इसमें है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की धारा 21 के तहत प्रदत्त ‘जीने के मूलभूत अधिकार’ की जो व्याख्या करते हुए जलवायु परिवर्तन शमन एवं रोजगार सृजन को भी उसमें शामिल किया है, भारत सरकार उसे क्रियान्वित कर प्रकृति केंद्रित न्याय को सभी प्राणियों के लिए सुरक्षित करे।
आईआईटी-खड़गपुर से सिविल-इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर राहुल बनर्जी पश्चिमी मध्यप्रदेश में लंबे समय से सामाजिक कार्यों, कृषि और शोध में लगे हैं।
साभार : सप्रेस